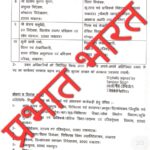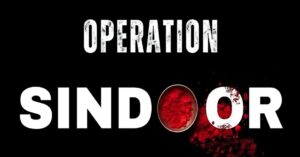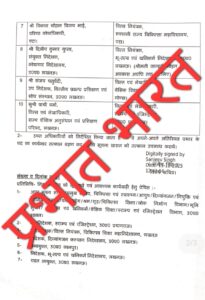(विजय प्रताप पाण्डेय) लखनऊ। आपातकाल (1975-77) भारतीय राजनीति का वह काला अध्याय है, जिसने देश के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, और जनता के अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला। यह वो समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों के बीच संविधान के अनुच्छेद 352 का हवाला देकर आपातकाल की घोषणा की। इसके तहत नागरिक अधिकारों का निलंबन, सेंसरशिप, और राजनीतिक असहमति का दम घोंटना प्रमुख था। आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद, 25 जून 1975 को, इंदिरा गांधी की सरकार ने कई विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भी प्रमुख था।
आरएसएस पर प्रतिबंध और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि
आरएसएस का गठन 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन करना और उसे मजबूत बनाना था। स्वतंत्रता के बाद, आरएसएस ने खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव और संबंध हमेशा विवाद का विषय रहे। जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रूप में उभरा, आरएसएस का राजनीतिक दल था और संघ के विचारों को राजनीतिक मंच पर लाने में इसका बड़ा योगदान रहा।
आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम (डीआईएसआईआर) का उपयोग करते हुए आरएसएस और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी की सरकार को आरएसएस और जनसंघ से राजनीतिक चुनौती मिल रही थी, क्योंकि ये संगठन उनके विरोध में सक्रिय थे और कांग्रेस की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे। जनसंघ के नेताओं और आरएसएस के स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या को इस समय गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) के उत्तराधिकारी, एमडी देवरस, को भी नागपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान जेल में रखा गया।
मीसा और डीआईएसआईआर: कानून का दुरुपयोग
मीसा (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम) और डीआईएसआईआर (भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम) का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चलाया। इन कानूनों का इस्तेमाल असहमति को दबाने और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालने के लिए किया गया। मीसा के तहत, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए और बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन रूप से हिरासत में रखा जा सकता था। आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई भी इसी अधिनियम के तहत की गई। संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे आपातकाल के विरोध में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे और सरकार के खिलाफ जनता को भड़का रहे थे।
आरएसएस और उसके साथ जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाना इंदिरा गांधी के लिए एक राजनीतिक रणनीति थी, क्योंकि संघ और जनसंघ का एक मजबूत समर्थन आधार था, जो उनकी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ मिलकर आंदोलन चला रहा था। आपातकाल के दौरान, संघ के स्वयंसेवक भूमिगत आंदोलन में सक्रिय थे, और उन्होंने गुप्त रूप से सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने, जनसभाओं का आयोजन करने और आपातकाल के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने का कार्य किया।
जेल में बंद स्वयंसेवक और आरएसएस का दावा
आपातकाल के दौरान आरएसएस के कितने स्वयंसेवक जेल में बंद किए गए थे, इसका सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। संघ और उससे जुड़े संगठनों का दावा है कि आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से अधिकांश संघ के सदस्य थे। हालांकि, इस दावे को सत्यापित करना मुश्किल है, आरएसएस का यह दावा उनके संगठन की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को महिमामंडित करने का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघ के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे।
सरसंघचालक एमडी देवरस की गिरफ्तारी और उनका जेल में रहना संघ के लिए एक बड़ा आघात था। जेल में रहते हुए देवरस ने कई बार इंदिरा गांधी को पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने आपातकाल की नीतियों और कार्यों की आलोचना की। उन्होंने यह भी कहा कि संघ एक गैर-राजनीतिक संगठन है और उसे इस विवाद से अलग रखा जाना चाहिए। हालांकि, इंदिरा गांधी की सरकार ने इन पत्रों पर ध्यान नहीं दिया, और संघ पर लगा प्रतिबंध आपातकाल समाप्त होने तक जारी रहा।
आपातकाल के बाद संघ की राजनीति में भूमिका
आपातकाल की समाप्ति और 1977 में आम चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (जनसंघ के उत्तराधिकारी) और आरएसएस ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा में कदम रखा। जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद, संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ी, और आरएसएस की छवि एक ऐसे संगठन की बनी जिसने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया।
आपातकाल के बाद संघ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब वह केवल एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा था। भाजपा, जो संघ के विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल थी, ने 1980 के दशक में तेजी से राजनीतिक क्षेत्र में अपना आधार मजबूत किया। संघ ने भी हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया और भारतीय राजनीति में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।
हिंदुत्व आंदोलन में आपातकाल की भूमिका
आरएसएस और हिंदुत्व विचारधारा के नेताओं के लिए आपातकाल एक निर्णायक क्षण था। इस अवधि को संघ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया, जब उसने राजनीतिक तानाशाही और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि आपातकाल के खिलाफ संघ का संघर्ष एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों और भारतीय समाज की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।
आरएसएस के इतिहास में आपातकाल को एक संघर्ष और विजय की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपातकाल के दौरान जो संघर्ष हुआ, वह संघ की विचारधारा और उसके कार्यकर्ताओं की दृढ़ता का प्रतीक है। संघ के लिए यह समय केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि यह उसके लिए एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें उसने अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी।
आपातकाल का दौर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण समय था। इस अवधि ने न केवल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हिला दिया, बल्कि कई संगठनों और नेताओं के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आरएसएस और उसके साथ जुड़े संगठनों ने इस समय के दौरान जिस संघर्ष का सामना किया, वह उनके इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने संघ को एक नए दृष्टिकोण से अपनी भूमिका का मूल्यांकन करने और भारतीय राजनीति में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।
आपातकाल के बाद, संघ और उसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कीं। आज, जब हम भारतीय राजनीति को देखते हैं, तो आपातकाल और उस समय की घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये घटनाएं भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के विकास की दिशा को प्रभावित करती हैं।