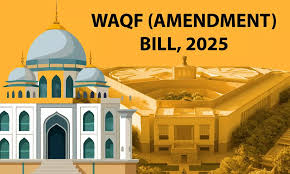सम्मान के साथ मरने का अधिकार: कानूनी होने के बावजूद क्यों चुनते हैं इतने कम लोग?
(विजय प्रताप पांडे ) भारत में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जीवन के अंतिम चरण में सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी। इसके तहत मरणासन्न मरीज या उनके देखभाल करने वाले जीवन-रक्षक उपकरणों को हटाने या उपचार को रोकने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन, कानून के बावजूद, बहुत कम लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जीवन के अंत की देखभाल (End of Life Care – EOLC) एक ऐसा विषय है, जो नैतिक, सामाजिक, कानूनी, और चिकित्सा के पहलुओं को एकसाथ जोड़ता है। यह न केवल मरीजों के लिए, बल्कि उनके परिवारों, डॉक्टरों, और समाज के लिए भी एक जटिल और संवेदनशील विषय है।
यह लेख उस मानसिकता, चिकित्सा प्रथाओं, कानूनी बाधाओं, और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर प्रकाश डालेगा, जो सम्मानजनक मृत्यु के कम स्वीकार किए जाने के पीछे हैं। साथ ही, यह विचार करेगा कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करके जीवन के अंत की देखभाल को व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है।
डॉ. रजनी सुरेंदर भट की कहानी: एक दुर्लभ उदाहरण
बेंगलुरु स्थित पल्मोनोलॉजिस्ट और पैलिएटिव मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. रजनी सुरेंदर भट ने हाल ही में एक परिवार की कहानी साझा की, जो जीवन के अंत की देखभाल के कठिन निर्णयों का सामना कर रहा था। 80 वर्षीय बुजुर्ग, जो डिमेंशिया और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से पीड़ित थे, बार-बार संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होते रहे। इस बार, उनके परिवार ने अस्पतालों और उपचार के बजाय, अपने प्रियजन की पीड़ा को समाप्त करने के बारे में सोचा।
डॉ. भट ने परिवार को समझाया कि वे अपने प्रियजन के जीवन समर्थन को हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। इस निर्णय ने उन्हें मरणासन्न देखभाल के साथ अपने प्रियजन को सम्मानपूर्वक अलविदा कहने का अवसर दिया। यह कहानी दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में, परिवार और डॉक्टरों को इस विकल्प के बारे में जानकारी नहीं होती है, या वे इसे अपनाने से हिचकिचाते हैं।
जीवन के अंत की देखभाल: एक कानूनी अधिकार
भारत में “सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार” कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग मामले की सुनवाई के दौरान निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिसके बाद 2018 में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव (AMD) या “लिविंग विल” की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिली। AMD के तहत, मरणासन्न रोगी पहले से ही यह निर्णय ले सकता है कि जब वह किसी इलाज या जीवन रक्षक उपचार को आगे नहीं चाहता, तो उसे वापस ले लिया जाए।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु का मतलब है कि जीवन को जबरन लंबा करने वाले उपचार को रोका जाए या हटाया जाए, जिससे व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो सके। यह फैसला परिवार को मानसिक, भावनात्मक, और शारीरिक रूप से कठिन उपचार प्रक्रियाओं से बचने का मौका देता है।
लेकिन सक्रिय इच्छामृत्यु, जो डॉक्टर के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से मृत्यु लाने की प्रक्रिया है, भारत में अभी भी अवैध है। इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जान-बूझकर मारने का कार्य नहीं कर सकते, भले ही यह व्यक्ति की इच्छा हो।
जीवन के अंत की देखभाल को अपनाने में कानूनी जटिलताएँ
हालांकि जीवन के अंत की देखभाल कानूनी रूप से स्वीकृत है, लेकिन इसे अपनाने में कई कानूनी जटिलताएँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन समर्थन हटाने की प्रक्रिया के लिए एक तीन-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया था। इसमें शामिल था:
1. प्रारंभिक राय के लिए एक आंतरिक चिकित्सा बोर्ड।
2. जिला कलेक्टर द्वारा गठित एक समीक्षा बोर्ड।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम भौतिक सत्यापन।
यह प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली थी, जिसके कारण इसे लागू करना मुश्किल साबित हुआ। जनवरी 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ प्रावधानों को हटा दिया, जैसे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति और जिला कलेक्टर की आवश्यकता। लेकिन फिर भी, यह प्रक्रिया लोगों को बहुत कठिन और लंबी लगती है, जिसके कारण बहुत कम लोग इस विकल्प को चुनते हैं।
सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएँ
भारत में मृत्यु को लेकर बहुत गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएँ हैं। भारतीय समाज में, परिवार को जीवन के हर पहलू में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और मृत्यु को एक संवेदनशील और धार्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। मृत्यु से संबंधित निर्णय लेना, विशेष रूप से जीवन समर्थन को हटाने का निर्णय, एक भावनात्मक और धार्मिक पहलू से जुड़ा हुआ है।
अधिकांश भारतीय परिवार मानते हैं कि जीवन को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए, भले ही मरीज को पीड़ा हो रही हो। यह सोच कि किसी के जीवन समर्थन को बंद करना गलत है, बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। कई बार, परिवार सोचता है कि जीवन समर्थन हटाने का निर्णय लेने से वे अपने प्रियजन की “हत्या” कर रहे हैं, जबकि वे सिर्फ उनकी पीड़ा को समाप्त करना चाहते हैं।
चिकित्सा जगत की जिम्मेदारी
चिकित्सा जगत में भी जीवन के अंत की देखभाल को लेकर स्पष्टता और जागरूकता की कमी है। ज्यादातर डॉक्टर इस विषय पर बातचीत करने से हिचकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे कानूनी या सामाजिक समस्याएँ हो सकती हैं। कई डॉक्टर अपने मरीजों के परिवारों को इस विकल्प के बारे में जानकारी नहीं देते, क्योंकि वे खुद इस प्रक्रिया से अज्ञात होते हैं या इसे अपनाने में झिझकते हैं।
डॉ. ई. दिवाकरन, जो त्रिशूर में दर्द और उपशामक देखभाल सोसायटी के निदेशक हैं, कहते हैं कि जीवन के अंत की देखभाल को अपनाने के लिए “मृत्यु साक्षरता” की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि डॉक्टरों और मरीजों दोनों को यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन के अंत की देखभाल क्या होती है, और इसका उद्देश्य मरीज की पीड़ा को कम करना होता है, न कि उनकी जीवन को जबरदस्ती खत्म करना।
“निष्क्रिय इच्छामृत्यु” बनाम “अंग समर्थन वापस लेना”: नामकरण का प्रभाव
डॉक्टरों का मानना है कि “निष्क्रिय इच्छामृत्यु” या “जीवन रक्षक प्रणाली वापस लेना” जैसे शब्द भ्रमित कर सकते हैं। इन शब्दों के उपयोग से ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे डॉक्टर रोगी को मारने की प्रक्रिया में शामिल हैं, जो कि सच नहीं है। इसलिए, डॉक्टरों का सुझाव है कि इसे “अंग समर्थन वापस लेना” या “उपशामक देखभाल” कहना अधिक सटीक और उपयुक्त होगा।
नामकरण का फर्क इसलिए पड़ता है, क्योंकि जब शब्द अधिक सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तो लोग उन्हें अधिक आसानी से समझते और स्वीकारते हैं।
जीवन के अंत की देखभाल की दिशा में आगे का रास्ता
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अंत की देखभाल के कानूनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है, फिर भी इसे व्यवहार में लागू करने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके लिए सबसे पहले, डॉक्टरों और मरीजों के बीच खुली बातचीत होनी चाहिए। डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने मरीजों और उनके परिवारों को सही समय पर सही जानकारी दें, ताकि वे कठिन निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार कर सकें।
इसके अलावा, समाज में भी इस विषय पर अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है, और इसके प्रति संवेदनशीलता और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है।
भारत जैसे समाज में, जहां परिवार और धर्म का विशेष स्थान है, वहां जीवन के अंत की देखभाल को स्वीकारना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। लेकिन जागरूकता, शिक्षा, और संवाद के माध्यम से, इसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है।
प्रभात भारत विशेष
भारत में सम्मान के साथ मरने का अधिकार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसे अपनाने की दर अभी भी बहुत कम है। इसका कारण कई स्तरों पर पाया जा सकता है – कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता, समाज में मृत्यु के प्रति धारणाएँ, और चिकित्सा समुदाय में जागरूकता की कमी।
फिर भी, इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मरीज और उनके परिवार समझ सकें कि जीवन के अंत की देखभाल क्या होती है, और उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार मिले कि वे किस प्रकार से मरना चाहते हैं। डॉक्टरों, कानूनविदों, और समाज के सभी लोगों को इस दिशा में सहयोग करना होगा ताकि जीवन के अंत की देखभाल का अधिकार वास्तव में सभी तक पहुंच सके।